
Loading...

Loading...
कुँवर सिंह ने छत्तीसगढ़ के पेण्ड्रा जिले के खोडरी खोंसरा गाँव में रहते हुए 2007 में बारहवीं पास की। फिर स्थानीय शिक्षक कृष्णानन्द पांडे ने रायपुर के घासीदास महाविद्यालय जाने के लिए कहा। पर वहाँ कला विषय लेकर कुँवर ने कोई तीन महीने ही पढ़ाई की। मन नहीं लगा। उन्हें यही सवाल परेशान करता रहा कि क्यों पढ़ना। कृष्णानन्द ने रायपुर में ही छत्तीसगढ़ एजुकेशनल रिसर्च सेंटर में काम लगवा दिया। यहाँ राजस्थान की दिगंतर संस्था, विद्याभवन सोसायटी और मध्यप्रदेश की संस्था एकलव्य के लोग मिलकर डीएड के पाठ्यक्रम बनाने के काम में जुटे थे। यह 2008 का साल था। यहाँ गेस्ट हाउस का प्रबंधन और खाना तैयार करना कुँवर की जिम्मेदारी थी। यहाँ संस्थाओं के प्रतिनिधि आते थे और रुकते थे। वे सुबह और रात गेस्ट हाउस में ही मीटिंगें करते। शिक्षा के व्यापक मुद्दों के बारे में कुँवर को यहीं से खबर लगी। उनकी चर्चाएं सुनने में कुँवर को मजा आने लगा। सवाल भी कौंधने लगे। कभी कभी हिम्मत करके कोई सवाल पूछ भी लेता पर सीधा कोई जवाब मिलता न था। उसे किताबें पढ़ने के लिए दे दी जाती थीं। कुँवर किताबें लेता तो था, पर पढ़कर समझना मुश्किल हो रहा था। चर्चाएं सुनने से ज्यादा समझ में आ रहा था। शिक्षा के बारे में जॉन हॉल्ट, गिजुभाई, मारिया मोंटेसरी, गांधी, टैगोर के विचार और बच्चों के सीखने को लेकर अलग अलग सिद्धांत यहीं सुनने-जानने को मिले। बार बार यही लग रहा था कि ये जो बातें यहाँ रायपुर में हो रही हैं वो मेरे गाँव खोडरी खोंसरा के स्कूल तक कैसे पहुंचेंगी?
2012 में रायपुर में एकलव्य का पिटारा खुला। पिटारा की जिम्मेदारी भी कुँवर को मिली। पिटारा का डिस्प्ले करना होता था। विभिन्न ट्रेनिंग में जो शिक्षक और मास्टर ट्रेनर आते उन्हें किताबें दिखाना और डीएड के कोर्स से उन किताबों का जुड़ाव बताना उनका काम था। इन्हीं किताबों से सामग्री लेकर डीएड की किताबें बनाई गईं थीं। यह ज्यादातर शिक्षा साहित्य था। ‘बच्चे असफल कैसे होते हैं’, ‘अध्यापक के नाम पत्र’, ‘उत्पीड़तों का शिक्षा शास्त्र’, ‘तोत्तो चान’, ‘दिवास्वप्न’, एकलव्य की ‘प्राशिका’, ‘पहला अध्यापक’। इन किताबों को कुँवर ने सरसरी तौर पर पढ़ रखा था ताकि इनके बारे में कुछ कुछ बताया जा सके।
अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कुँवर ने इग्नू से बीए किया। कुँवर बताते हैं यह बीए भी उन्होंने बड़े ही बेमन से किया क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य कुछ समझ में नहीं आता था। तीन साल का कोर्स छह साल में भी पूरा नहीं हुआ। दो पेपर रह गए तो रह ही गए।
2018 में छतीसगढ़ से मध्यप्रदेश के भोपाल आना हुआ। यहाँ एकलव्य का पिटारा ज्यादा विस्तृत और समृद्ध था। कुँवर का कहना है कि यहाँ बाल साहित्य ज्यादा था, पर बच्चों की किताबें पढ़ने के बारे में बड़ा ही सतही नजरिया था। जल्दी से कहानी खत्म। थोड़ा मजेदारी थी पर जुड़ाव नहीं बनता था क्योंकि ठहराव ही नहीं था। न तो कहानी की कहन पकड़ में आती, न किरदारों की बनावट और न चित्रों के कोई अर्थ खुलते। लगता बच्चों की कहानी में क्या धरा है, क्योंकि आँखों में तो शिक्षा साहित्य का चश्मा चढ़ा हुआ था।
2019-20 में पिटारा की पूरी जिम्मेदारी आने पर, किताबें बेचने के लिए, किताबों के बारे में बताना, प्रकाशनों व कंटेन्ट की जानकारी रखना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। पढ़ने में मजा आता तो यही लगता कि पुस्तकालय स्कूल में होना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ बात समझ न आती थी।
यहाँ एकलव्य के परिसर में ही पराग के एलईसी कोर्स का कान्टैक्ट होने के कारण प्रतिभागी यहाँ पिटारा में आते और किताबों के बारे में चर्चा करते। कुछ प्रतिभागी देर रात तक पिटारा में बैठकर किताबों को देखते और सत्रों में जो बात हुई होगी उसका संदर्भ रखते हुए चर्चा करते। मुझे बड़ा अच्छा लगता और मैं उनकी बातें सुनता हुआ बैठा रहता। उनके जाने के बाद मैं उन किताबों को उठाकर देखता पर मुझे कुछ खास समझ न आता।
चूँकि एलईसी के कान्टैक्ट में खुलापन था इसलिए कभी कभी मैं गेस्ट फेकल्टी के सत्र में जाकर बैठ जाता था और वहाँ बातें सुनता। कविताओं पर सुशील शुक्ल का सत्र था। बाल साहित्य की इतनी गूढ़ बातें मैंने कभी सुनीं भी नहीं थीं। कविताओं में कहन की बारीकी, छुपा हुआ अर्थ और भाषा का खेल मैंने पहली बार जाना। मैंने सैद्धांतिक बातें सुन और समझ रखीं थीं पर किसी कविता के उदाहरण से उसके संसार के खुलने की बात यहाँ समझ में आई।
यह सब देखते सुनते मेरे भी मन में खयाल आया कि जब बाल साहित्य का प्रमोशन का काम करना ही है, पिटारा संभालना ही है तो क्यों न पुस्तकालय और बाल साहित्य की समझ बनाने के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या कोर्स कर ही लिया जाए। मैंने संस्था में अपनी बात रखी। सहमति बनी और मैंने एलईसी के लिए ऐप्लीकेशन भर दिया। लेकिन उस साल मेरा चयन नहीं हुआ। थोड़ा निराशा भी हुई पर एलईसी कान्टैक्ट के सत्रों में जाना और बैठकर चर्चाएँ सुनना मैंने बंद नहीं किया। ट्रेनिंग हाल में किताबें जमाने और लाइब्रेरी डिस्प्ले बनाने के लिए मैं भी फेकल्टी के साथ लगा रहता था।
अंततः 2021 के एलईसी बैच में शामिल होने का मौका मिल ही गया। पहले कान्टैक्ट के पहले ही सत्र रीडिंग जर्नी के दौरान जब दो पसंदीदा किताबें और उनके लेखकों के नाम बताने की बारी आई तो पहले तो काफी देर तक कुछ सूझा ही नहीं, फिर किताबों के नाम तो लिख लिए पर उनके लेखकों के नाम याद ही न आए। समझ में आया कि किताबों के साथ उनके लेखकों को जानने का भी एक संसार है। इसी तरह चित्रकार का नाम भी जेहन में कभी चढ़ा ही नहीं। पढ़ा हुआ सब अधूरा जान पड़ा। सिर्फ कहानी याद रह गई थी। अब यह समझ में आ रहा था कि लेखक को जानने का क्या महत्व है। लेखक और उसकी किताबें जानने से यह समझ पुख्ता होती है कि इस तरह की किताबें लिखने वाले ये हैं, इनकी शैली उनसे मिलती है, किनसे अलग है इनकी शैली, कैसी शैली है; यह साहित्य का पूरा संसार है। इसे भी जानने की जरूरत है। कोर्स के दौरान किताबों को उलटते पलटते अब मैं यह भी देखने लगा था।
इसी तरह किताबों को मैं सिर्फ तीन केटेगरी में ही जानता था। पिटारा में किताबों के बीच मेरी जो समझ बनी थी उसमें ‘कहानी’, ‘कविता’ और ‘गतिविधि किताबें’ ही सबकुछ था। कोर्स में साहित्य की विधाओं का विस्तार खुला। किताबों के संसार के बीच रहने वाले एक इंसान के लिए जैसे खजाना हाथ लग गया था। अब मैं पिटारा में बैठकर विधाओं की पड़ताल करता। यात्रा वृतांत, जीवनी, ग्राफिक नॉवेल, कान्सेप्ट बुक, विज्ञान अवधारणा, साइंस फिक्शन। मैं बाल साहित्य में सिर्फ कहानी- कविता को ही सबकुछ मानकर चल रहा था। पर साहित्य तो सबके लिए है तो बच्चों के साहित्य में भी यह सब है ही। बस देख नहीं पा रहा था मैं। मैं इन सबको कहानी की तरह ही देख रहा था। यह सच्ची घटना है, किस तरह की सच्ची है और इसका फॉर्मैट क्या है, यह सब देखने लगा मैं।
कहानी की किताबों की वकालत के लिए कल्पनाशीलता, तार्किक चिंतन, मानवीय मूल्य, संवेदना, जीवन कौशल आदि बिन्दु सुन रखे थे पर यह सब होगा कैसे, यह एलईसी कोर्स के सत्रों के दौरान किताबों पर बारीक नजर डालने और चर्चाओं से समझ में आया। अलग अलग तरीकों से सुनाई गई कहानियाँ, कहानी की परतों में झाँकना, पात्रों की स्थितियों को समझना, लेखक के नज़रिये को पकड़ना और एक पाठक की तरह खुद का नजरिया बनाना यह सबकुछ नया नया और रोमांचित करने वाला रहा।
कहानी पढ़कर मजा पहले भी लेता था पर चित्रों पर नजर न के बराबर जाती थी। यह सोचकर कि बच्चों की किताबों के चित्रों को क्या देखना, बस पढ़ते हुए पन्ने पलटता जाता था। लेकिन जब कोर्स के एक सत्र में चित्रों पर बारीकी से बात हुई, तो उसमें निहित परतें भी समझ में आयीं। चित्र सिर्फ चित्र नहीं पूरी कहानी थे, कहानी से आगे बढ़कर थे। चित्रों में तर्क, सामंजस्य, संपूर्णता और पूरकता दिखने लगी। चित्र भी आपका विचार बनाता है, उनको पढ़ना भी एक पढ़ना है, यह समझ में आया। एक ही किताब में ढेर सारी संभावनाएं है यह समझ में आया नहीं तो पहले कहानी खत्म होने पर किताब भी वहीं खत्म हो जाती थी। अब ठहराव आया है, किताब को फिर-फिर से देखने, सोचने-समझने और खोलने का शौक बना है।
कोर्स के बाद अब पिटारा में बैठे हुए मैं ज्यादातर किताबों को इन्हीं नजर से देखता हुँ। किताबों पर साथियों से चर्चा करता हुँ। खरीदी करने आए लोगों को किताबें सुझाता हूँ और उनके बारे में बारीकी से बता पाता हूँ।
जब चर्चाएं होती हैं तब भी इन किताबों पर फिर से लौटने का मन होता है। उदाहरण के लिए ‘मैं भी’, वी सुतेएव की एक छोटी सी कहानी है एक बत्तख और चूजे की। लेकिन इसमें भाषा का खेल, खुद से सोचने समझने के मौके, निर्णय लेने की समझ सबकुछ एकदम मौलिक रूप से है। कोई शिक्षक नहीं है, कोई अभिभावक नहीं है सिखाने के लिए, लेकिन सीखना हो रहा है। यह बात पहले इस तरह नहीं समझ में आती थी।
‘सो जा उल्लू’ में भी एक छोटी सी कहानी है। उल्लू सोना चाहता है, पर सारे जानवर जगा देते है। फिर जब सारे जानवर सो जाते हैं तो वह उन्हें जागा देता है। लेकिन चर्चा करते हुए अब उसमें बहुत सी परतें दिखती हैं। भाषा का खेल, शब्दों का दुहराव, अपनी अपनी बोली, और जंगल का एक भरा पूरा संसार। पहले इसी कहानी में बैर और द्वेष दिखता था, बदला लेने की बात दिखती थी, लेकिन अब अपनी-अपनी पहचान वाली बात और शरारत दिखाई देती है। उल्लू की भी और बकियों की भी।
कोर्स के बाद पहली बार मैंने एक किताब की समीक्षा लिखी। विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह ‘बना बनाया देखा आकाश, बनते कहाँ दिखा आकाश’ की समीक्षा ‘द बुक रिव्यू’ में प्रकाशित हुई। किताब को कई बार पढ़ा, उसकी छोटी छोटी कविताएं हर बार एक नया अर्थ खोलती। तब पढ़ने और पढ़कर समझने और समझकर अलग अलग बातों से जोड़ने का जादू समझ में आया।
अभी एकलव्य के “जश्ने तालीम’ कार्यक्रम से जुड़े 35 वालेन्टीयर्स की कार्यशाला में एक पूरा दिन किताबें पढ़ने और किताबों के साथ की जाने वाली गतिविधियों पर सत्र संचालित किए। गतिविधयो का डेमो दिया, समूह चर्चाएं कराईं। इसके लिए सत्रों की अच्छी तैयारी की और बहुत सारी किताबें पढ़कर उनके लिए गतिविधियां डिजाइन कीं।
इन्हीं वालेन्टीयर्स की एक दूसरी कार्यशाला में विधाओं पर एक विस्तृत सत्र लिया। उसकी तैयारी के दौरान विधाओं की समझ और उदाहरण और पक्के हुये। पुस्तकालय बनाने और चलाने पर भी बातचीत की। मृत्यु थीम पर ‘मेरी जोया चली गई’, ‘कीमिया’ और ‘आ आजो अब रात’ पर बातचीत के लिए सवाल और चर्चा के बिन्दु तैयार किये। बिल्कुल नया अनुभव रहा।
अभी हाल ही में स्कूल फॉर डेमोक्रेसी का एक शिक्षक समूह एकलव्य की विजिट पर आया तो उनके लिए ‘खुश खुश कछुआ’ पर बुक टॉक का डेमो दिया। पिटारा का टूर कराया और किताबों के बारे में जानकारी दी। अब किताबों की बारे में आत्मविश्वास से बात कर पाता हूँ क्योंकि किताबें अच्छी तरह पढ़ रखीं हैं और उनपर राय भी बनी है।
किताबों की मांग आती है तो जरूरत के अनुसार किताबों का सेट बनाने में अब मैं विधाओं की विविधता और गतिविधियों की संभावनाओं को आधार बनाता हूँ। अब मैंने अपने लिए पढ़ना शुरू किया है। किताबों को पढ़ते समय ठहरना, सोचना और फिर पलटकर पीछे जाना फिर से पढ़ना, दरअसल इसका मजा ही कुछ और है, पहले इससे वंचित था मैं।

There are many kinds of families around us. There are families we are born into, and families we become a part of. We love them, fight with them, and…
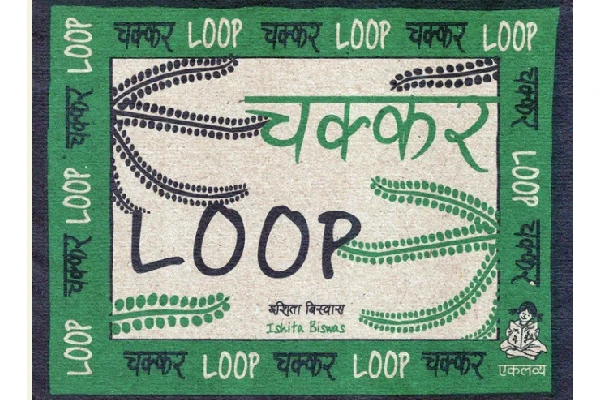
When Pictures Speak a Thousand Words
We often say that children’s literature is for everyone- it offers the imagination, the narrative and the richness that can appeal to readers of all…